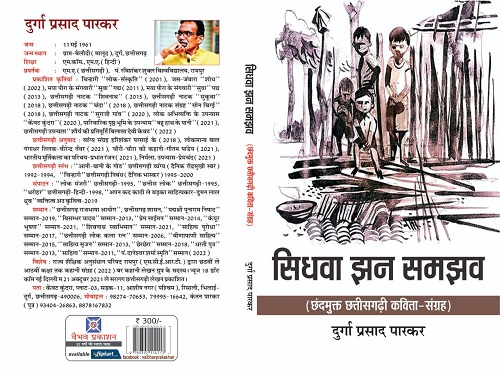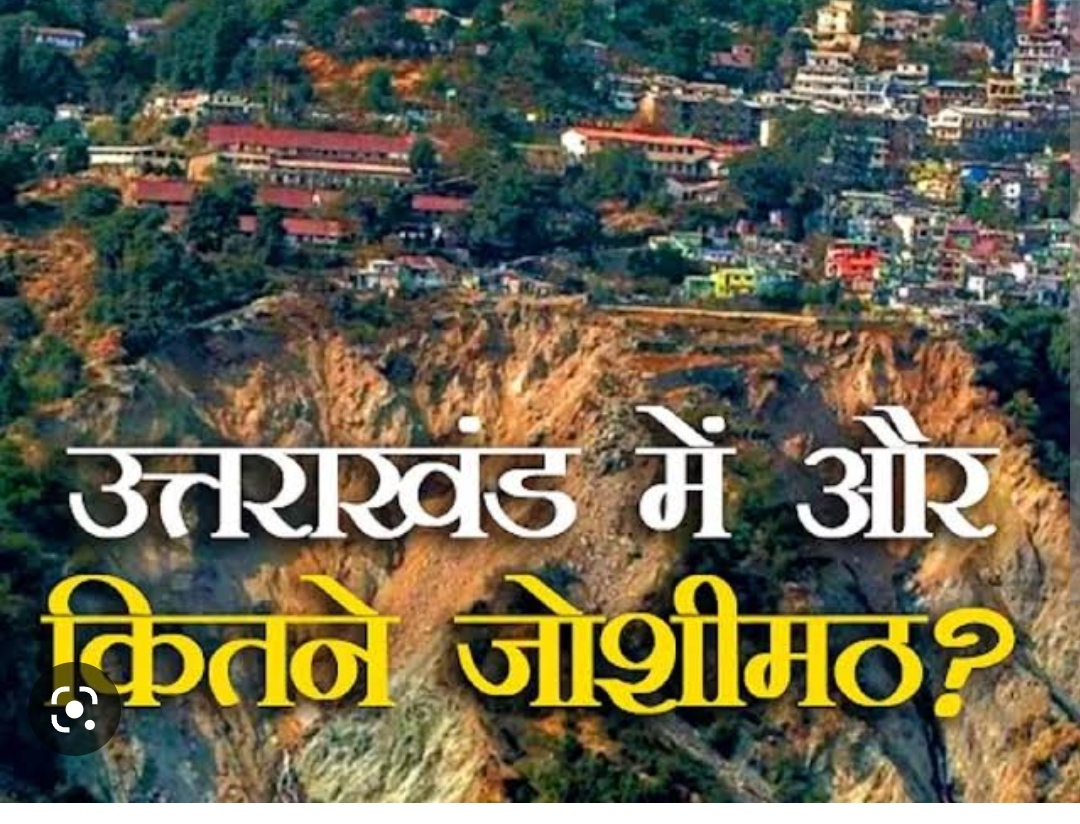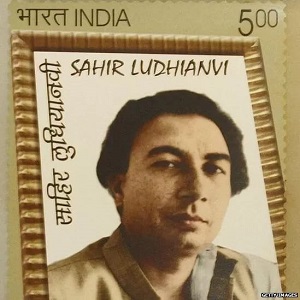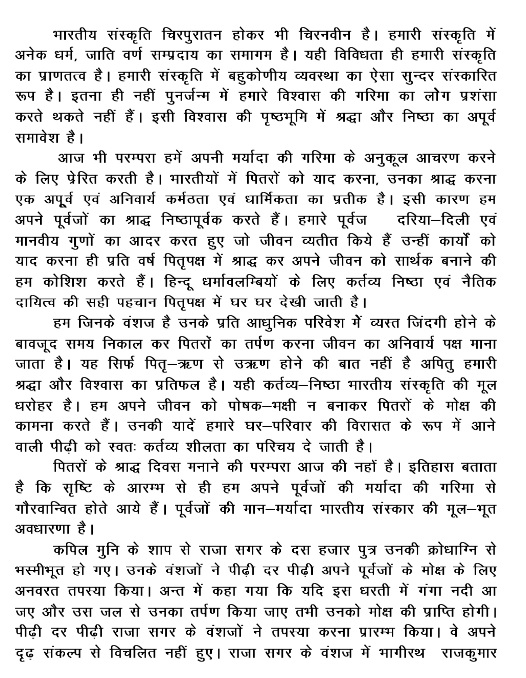- Home
- Chhattisgarh
- ■पुस्तक समीक्षा : ‘उस औरत के बारे में'[कविता संग्रह]. ■कवयित्री : डॉ. आशा सिंह सिकरवार. ■समीक्षक : प्रभा मजूमदार.


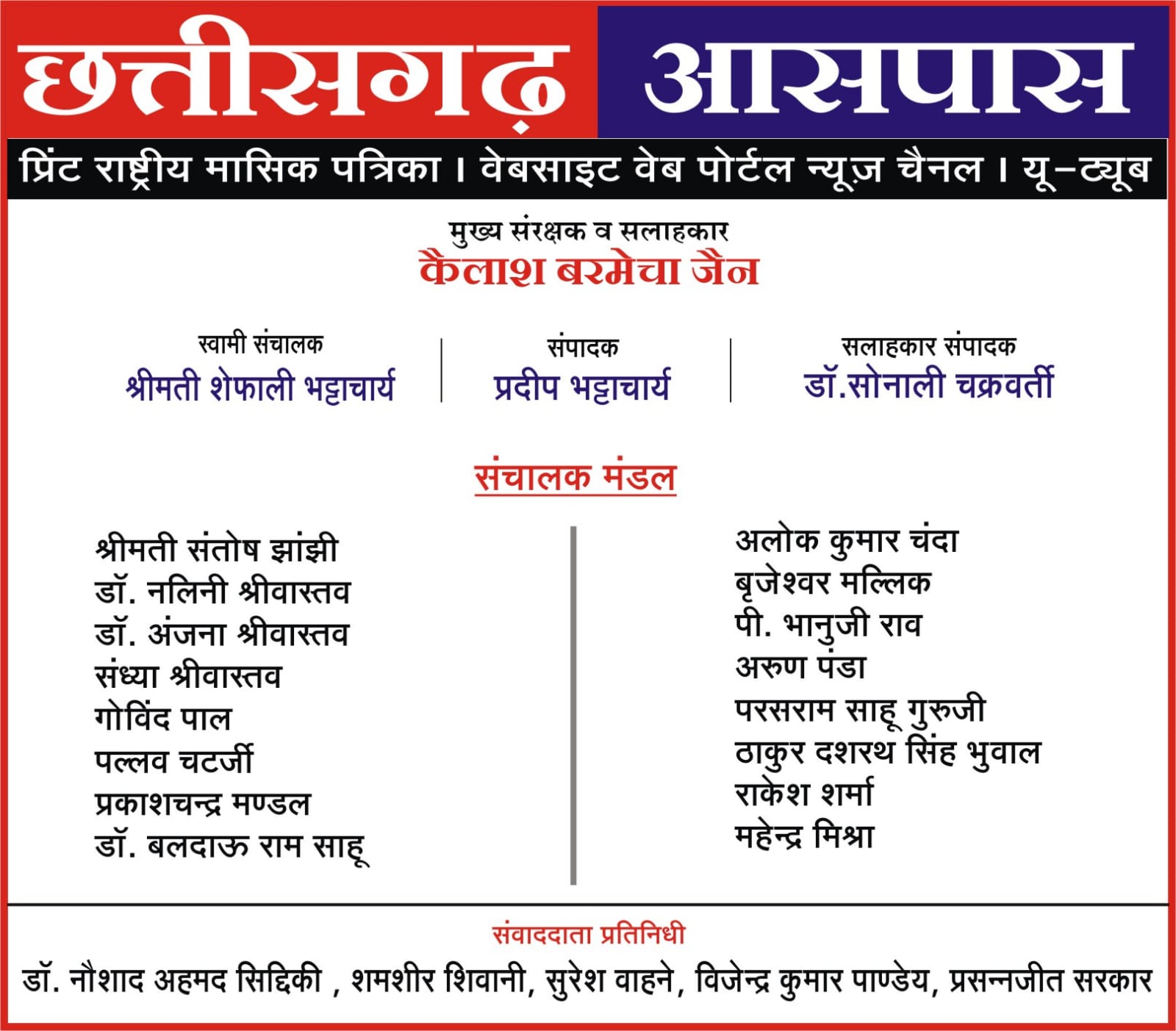





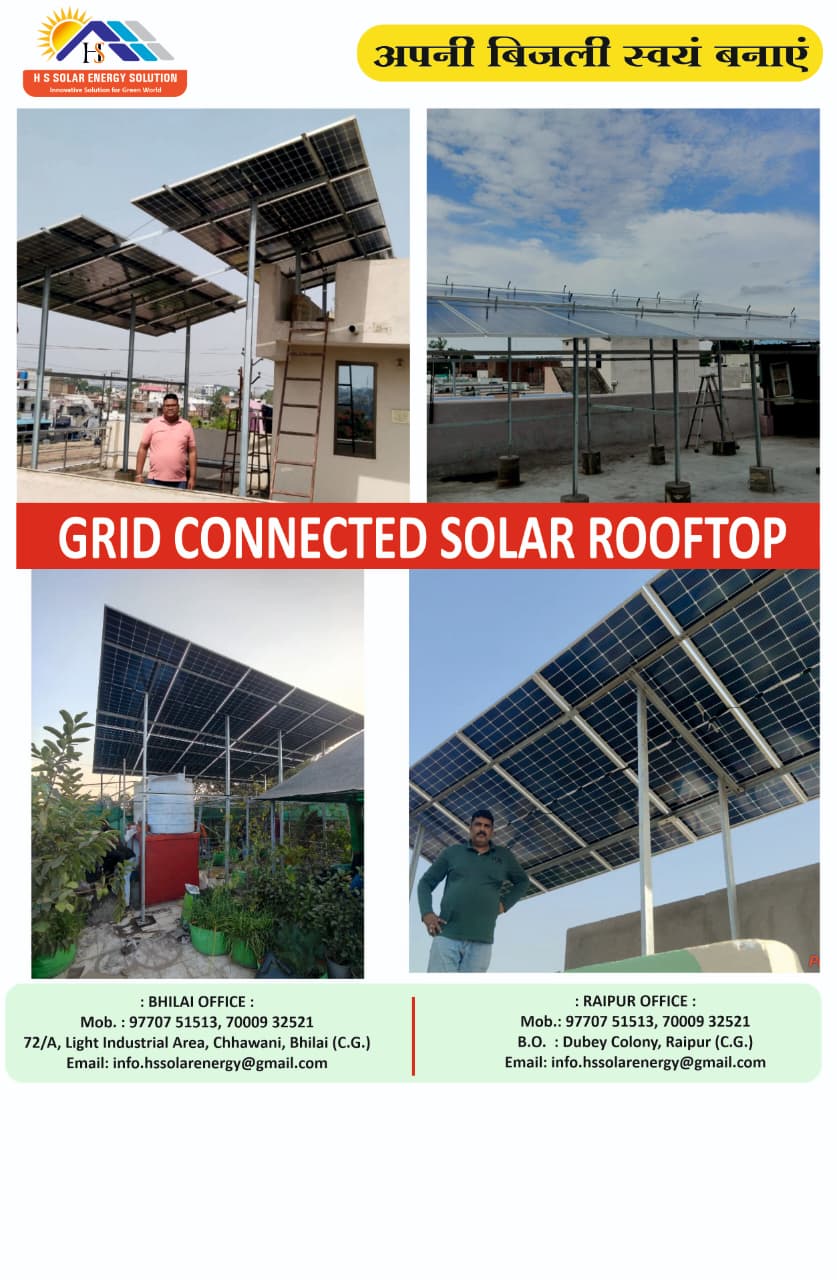

■पुस्तक समीक्षा : ‘उस औरत के बारे में'[कविता संग्रह]. ■कवयित्री : डॉ. आशा सिंह सिकरवार. ■समीक्षक : प्रभा मजूमदार.

■डॉ.आशा सिंह सिकरवार

■प्रभा मजूमदार
♀ उस औरत के बारे में : नई दुनिया की संरचना समीक्षा
स्त्री की वेदना, बैचेनी, छटपटाहट, संघर्ष और जिजीविषा को शिद्दत से अनुभूत एवं महसूस करती आशा सिंह की कविताएं स्त्री जीवन के हर पक्ष, पड़ाव एवं विषय पर अपनी बेबाक अभिव्यक्ति दर्ज करती है। स्त्री पुरुष सम्बन्धों को शोषण की बुनियाद पर होने, सामाजिक- पारिवारिक दबावों के चलते स्त्री के सपनों अरमानों के बिखरने , धार्मिक रूढ़ियों विधानों की तहत उन पर लादी गई आचार संहिताओं जैसे अनेक मुद्दों पर उन्होने लिखा है। आशा जी की कविताओं में संवेदनाओं की तरलता है तो ज्वालामुखी सा लावा भी है, अनेक परतों के नीचे धधकता हुआ। वे आह्वान करती हैं एक सार्थक प्रतिरोध का, पूरे बदलाव का, नई दुनिया की संरचना का। उनके कविता संग्रह “उस औरत के बारे में” में प्रेम, परंपरा, रूढ़ियों, सम्बन्धों, अपेक्षा दायित्वों और शोषण के अनेक स्तर बड़ी सूक्ष्मता और संवेदना के साथ दर्ज हुए है। वे स्त्री व्यथा का सार इन शब्दों में रखती हैं “वह हँसती है/ हृदय पर पहाड़ सा दुःख रख कर/ मानों दरक जाते हैं पहाड़/ चटकने लगती है हंसी/ छलकाने लगती है नदी” (गांठ)।
मुक्ति और सम्मान की चाह को अपनी पहली ही कविता में शब्द देती हैं और बंद कमरे में कैद वें गौरैया हो जाने की कामना करता हैं। दरअसल, पंखों में ताजगी भर अंबर में उड़ान भरती और अपने परिवार के साथ खाती- विश्राम करारी गौरैया उन्हें प्रेम, समर्पण और स्वतंत्रता का प्रतीक लगती है (गौरैया)।
एक आम औसत औरत की तमाम जिंदगी रोटियाँ सेंकते, कपड़ों से मेल छुड़ाते, पलकें झुका कर हर आदेश का पालन करने जैसी अनिवार्यताओं के बीच वें उसके अस्तित्व से जुड़े सवाल उठाती हैं और रूढ़ियों प्रतिष्ठा के नाम पर थोपे, देह पर लादे गए गहनों को मन आत्मा पर पड़ा बोझ (प्रतिरोध) कहने से नहीं हिचकती । इसी सिलसिले में उनकी अगली कविता “सिलविलिया” सबकी हथेली पर अमृत रखने के उस पर पड़े मानसिक सामाजिक दबाव के साथ ही व्रत तप जैसे विधान का षडयंत्र उजागर करती हैं। उन्हें आश्रिता बना रखने का यह षडयंत्र “आसरा” में और भी स्पष्ट होता है। निस्संदेह इस “यंत्रणा” के पीछे सामाजिक और धार्मिक मूल्य निहित हैं जो दमन और तिरस्कार की हिंसा को स्वीकृत और प्रतिष्ठित करते हैं। जिल्लत की रोटी” में तो वे उस औरत को प्रतिरोध का सीधे सीधे आह्वान करती हैं, जो सहनशीलता के नाम पर दैहिक भावात्मक शोषण और जानवरों की तरह दुतकार सहती है। चोट शीर्षक की छह कविताएं हैं जिनमें रचनाकर चोट के विभिन्न रंगों-प्रकारों- आकारों तथा अनेक परतों को यथार्थपरक तरीके से समझती है तथा चोट की मूल प्रवृत्ति इस तरह बयान करती हैं “ चौका बर्तन करते/ अवेरते हुए कपड़े/ झाड़ते-पोंछते/ चोटें कहाँ बिला जाती हैं” मगर कमर सीधी करने के वक्त जग जाती हैं। साथ ही उस मूक प्रतिरोध को नजरअंदाज नहीं होने देती “टपकती है अंगारों पर/ भीत के पीछे बसी/ प्रतिरिध की कोठारी/आंच और चोट का रिश्ता/ समानान्तर चलता है” और “दूर सुलगती हैं वे/ ठंडे चूल्हे सी बुझने को होती हैं”।
वे जिक्र करती हैं कितनी हीं अदृश्य “हथकड़ियाँ” होने का जो सुहागन के चिह्न के नाम, कभी धर्म-कर्म की रस्मों के नाम उन पर जकड़ दी गईं हैं और मजबूत प्रहारों के बगैर नहीं टूटेंगी। हथकड़ियों- दीवारों को तोड़ने के इसी प्रयोग और प्रहार करने वाली साहसी औरत की प्रतिष्ठा उन्होने “दीवारों के बारे में ) कविता में की है।
आशा जी की स्त्री अपनी पूर्व पीढ़ी से अलग है जो “अम्मा की तरह उम्र भर / कंडे नहीं थप सकती थी हम” और वे अपने पिता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हैं कि “हम भेड़- बकरियाँ नहीं हैं बाबा/ तुमहारे शरीर की लाल बूंदें हैं हम/ जो धूप के स्पर्श से/ दहक उठती हैं / गुलमोहर कि तरह (पंख वहीं रह गए)। इसके बावजूद मुक्त उड़ान के लिए पंख कट जाने का दुख उन्हें साल रहा है। नदी के प्रवाह में पत्थर को अवरोध मान कर वें, नदी को किनारों की सुरक्षा के मोह से मुक्त हो जाने का आह्वान करती हैं “पत्थरों का मौन” । बनी हुई मूरत को हथोड़े के वार से तोड़ कर, नई मूर्तियों की निर्मिति की कामना करती लेखिका पुरानी खोह से निकलने, सीमाएं तोड़ने की गुजारिश करती हैं “सीमाएं जब टूटती हैं”। ऐसी ही एक शुभ कामना है अंधकार कविता में “इस बार रोशनी की किरण/ आ गिरे मेरे आँगन में/ बज उठें साँसों के तर/ नवीन उद्गार/ नयी चेतना/ नवीन शाखाएँ फूटे”। हालांकि उसका दर्द है “लक्ष्मण रेखा पर करते ही/ सिर हथोड़े की चोट से/ लहूलहान हो गया” (दूसरी आँख) ।
अपनी जिंदगी और अस्तित्व के निर्णय स्वयं लेने को उकसाती उनकी पंक्तियाँ “याद रहे तुम बंदरिया नहीं हो/ जो मदारी के कहने पर/ तमाशबीन को सलाम ठोके/ और तालियों कि गड़गड़ाहट में भूल जाए/ कि अब तक उसकी लगाम/ मदारी के हाथ में है” (लगाम) ।
उनकी कविताएं वेदना विवशता यंत्रणा की ही नहीं हैं- एक चुनौती, प्रतिरोध, आक्रोश इनमें साफ पढ़ा और समझा जा सकता है। “पल्लू के छोर से पोंछते हुए नाक/ टपकती है अंगारों पर/ भीत के पीछे बसी/ प्रतिरोध की टोकरी/ आंच और चोट का रिश्ता/ समानान्तर चलता है”।
आशा जी का प्रतिरोध बेहद मुखर है। “औरत का शरीर क्या है? धँसते काँच के टुकड़े कलाइयों में/ इतना भर !! निश्चय ही वे इस नियति को अस्वीकार करती हैं और विद्रोह करते हुए, अपना रास्ता खुद तलाश करती हैं।
“मैंने भर दिया है उसमें
रणभूमि का उद्घोष
संसार की सभी औरतों को
अपने अकेलेपन में आमंत्रित करती हूँ “ (अकेलेपन में)
इसी तल्ख प्रतिरोध की निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं “वह जानती है तुम्हारे नाखूनों और दांतों के बारे में/ जानती है तुम्हारी जालसाजी और तिकड़मों के बारे में/ इस वक्त उसके हाथ में हंसिया है/ जानती है वह फसल के बारे में” (जानती है वह)।
उनकी संवेदना स्त्री की वेदना, तिरस्कार और प्रतारणा तक ही सीमित नहीं है। उन्हें हर वंचित का शोषण और अपमान आहत करता है तथा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी। आरी से काटे जा रहे पेड़ों के धरती पर गिरने, जंगलों के राख होने, मछलियों के तड़पने, पक्षियों के बेघर होने जैसी त्रासद स्थितियों, विध्वंसी कृत्यों और प्रकृति के विलाप को उन्होने “पेड़ पुकारते हैं” में दर्ज किया है।
साहूकारों सामंतों द्वारा शोषण और गिरवी रखी जमीन, बेघर मजदूरों का दर्द उन्हें बैचेन कर देता है “यह कैसी लड़ाई है”। हालांकि वे उम्मीद भी करती हैं “कुछ तो अंधेरा मिटेगा/ कुछ चीन्हेंगे रास्ते/ कुछ काफिले बनाएँगे/ कुछ मंजिलों तक पहुचेंगे”। उनकी भावना और कामना “जो नहीं देख प रहे है सूरज/ उनके लिए सूरज को/ अपनी हथेली पर उगाना चाहती हूँ” सराहनीय है।
कुल मिला कर डॉ आशा सिंह सिकरवार की का कविताएँ सशक्त एवं मुखर अभिव्यक्ति हैं। स्वयं लेखिका के शब्दों में- मानवीय संवेदना का धरातल और गहरा हो जाए, संवेदनात्मक जमीन में नमी रहे, एक दूसरे के लिए करुणा बनी रहे। इसके साथ ही व्यक्ति के सम्मान, न्याय एवं अधिकार से वंचित रह जाना उनके अंतस को कचोटता है और वे ऐसी स्थिति का प्रतिरोध कर एक समतली लड़ाई लड़ना चाहती हैं। तंत्र,व्यवस्था और लंबी परम्पराओं द्वारा निर्मित विद्रूपताओं के विरुद्ध लड़ाई साहस, संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ ही लड़ी जा सकती है और डॉ आशा सिंह इसके लिए समर्पित हैं “उनके संघर्ष में/ विपरीत परिस्थितियों में / लड़ने की शक्ति बनना चाहती हूँ मैं/ ताकि हजार हजार वर्षों तक/ पृथ्वी पर बचे रहें उनके चिह्न”।
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ आशा सिंह को, न्याय और समानता के लिए आरभ किए शंखनाद के लिए।
■कवयित्री संपर्क-
■78029 36216
◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
chhattisgarhaaspaas
विज्ञापन (Advertisement)







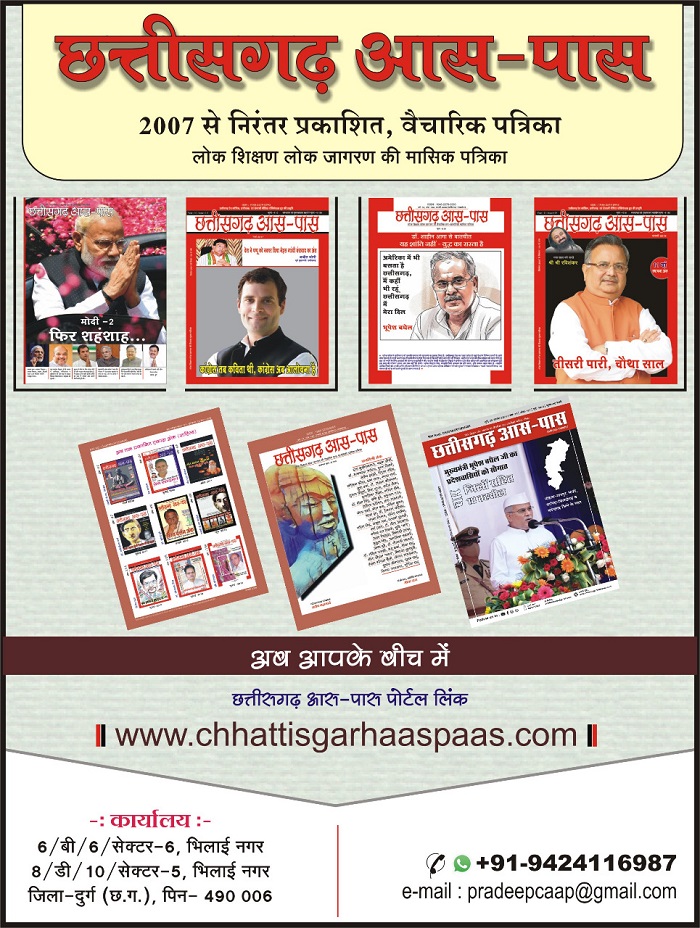























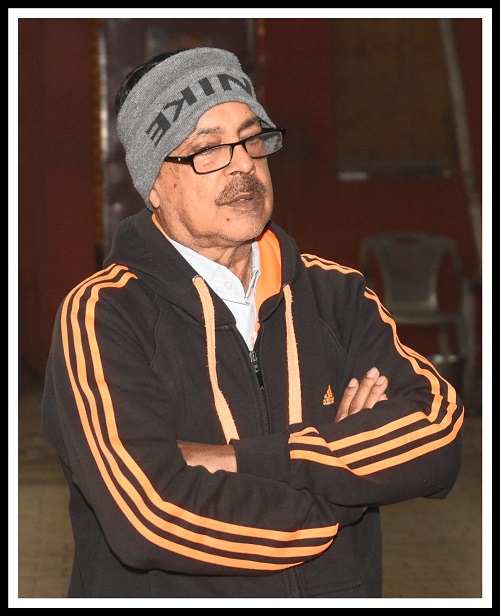
![होली विशेष [दो फागुनी रचना यें] – तारकनाथ चौधुरी](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-02-at-9.16.30-PM.jpeg)













![कविता आसपास : बसंत पंचमी पर महाकवि ‘निराला’ को याद करते हुए… महाकवि की वेदना…!! – विद्या गुप्ता [छत्तीसगढ़-दुर्ग]](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Image-2026-01-21-at-11.12.59-PM.jpeg)

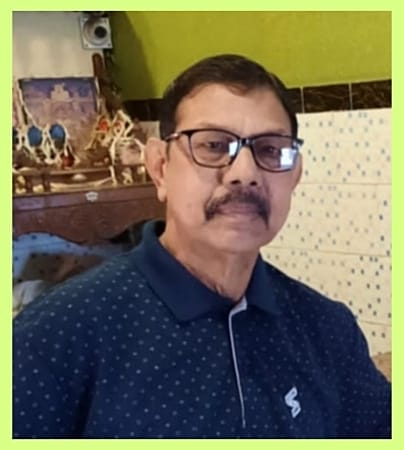








![मास्टर स्ट्रोक [व्यंग्य] : राजशेखर चौबे](https://chhattisgarhaaspaas.com/wp-content/uploads/2025/02/K-1.jpg)